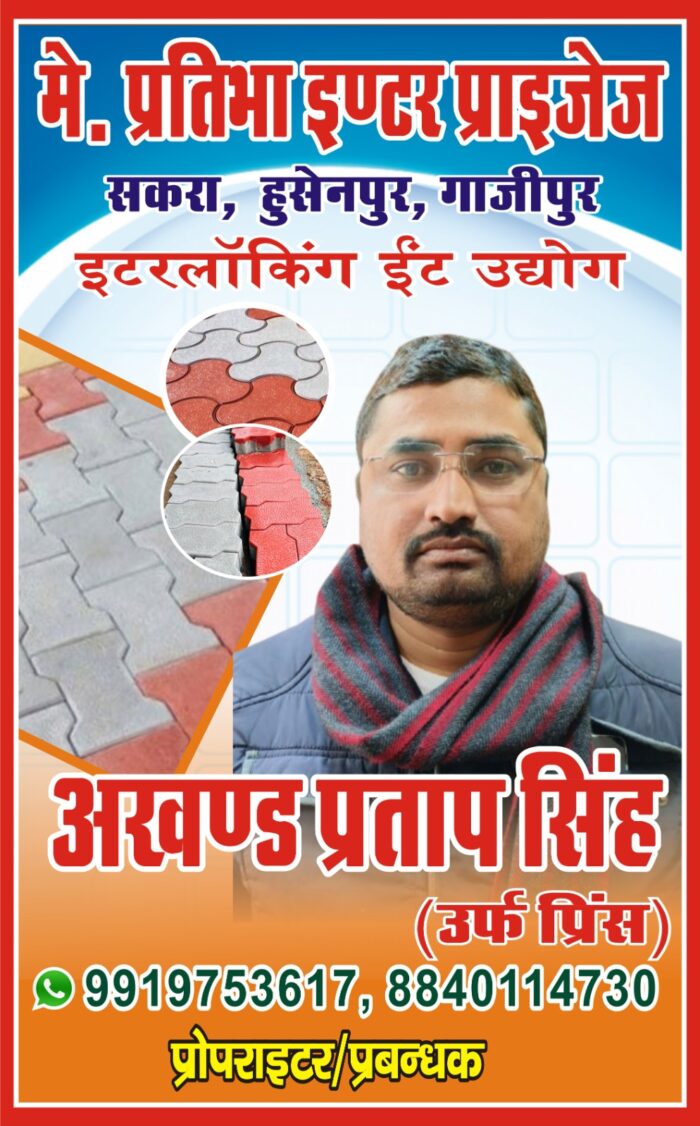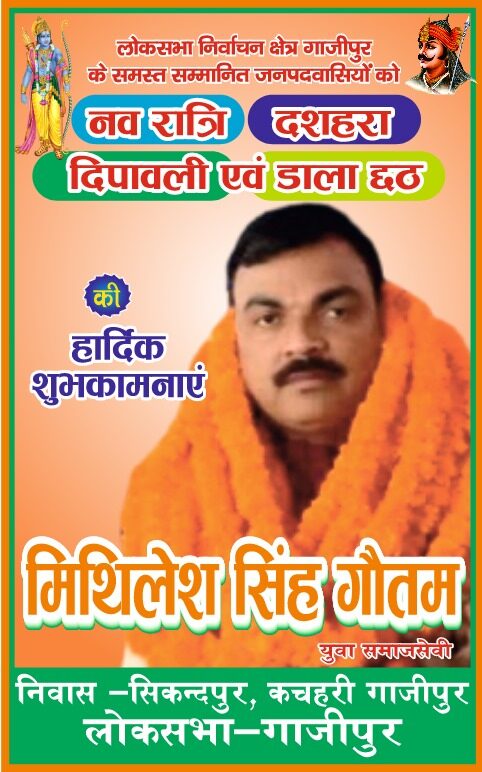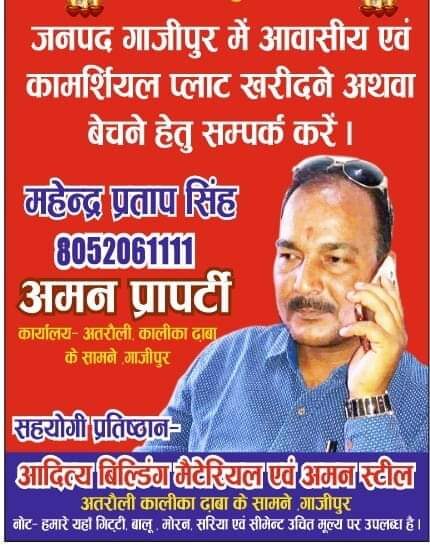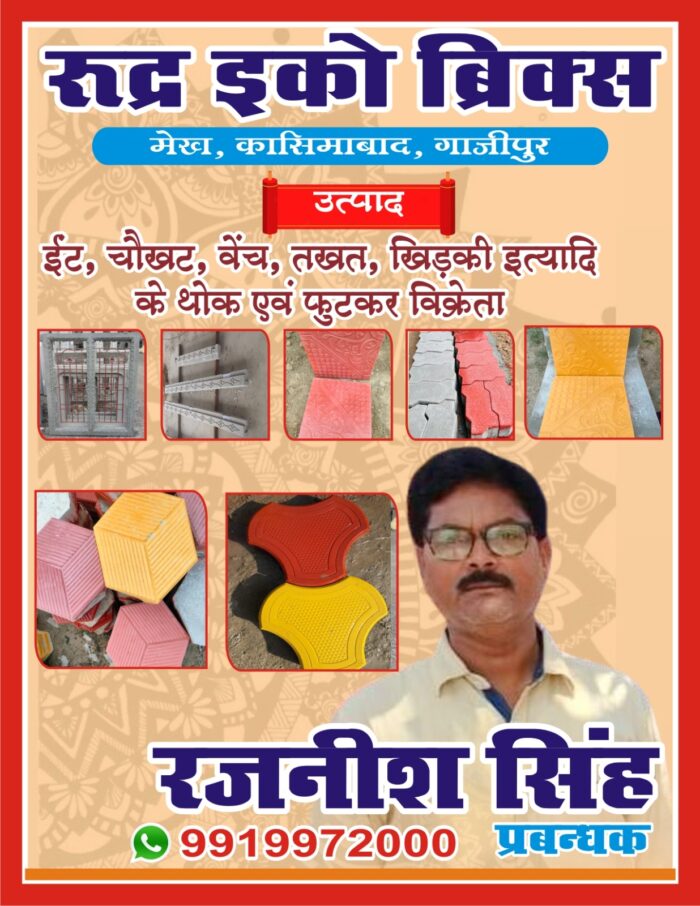गाजीपुर- झांके गोरी टारिके ओहार

गाजीपुर-इक्षु एकादश इग्यारह कवियों की भोजपुरी कविताओं का संकलन है. भोजपुरी समाज अपनी भाषा और संस्कृति को बाज़ार के हाथों में सौंप चुका है, इसलिए कुछ संवेदनशील लेखनियाँ निस्पन्द होते जा रहे भोजपुरी साहित्य में प्राण फूंकने का प्रयास कर रही हैं. यह सम्भव है कि अस्तित्व के संघर्ष में भोजपुरी साहित्य पीछे छूट रहा हो परन्तु अंतिम भोजपुरी रसिक अध्येता के अस्तित्व तक इसका अस्तित्व रहेगा. मोटे तौर पर आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में सोलह करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी भाषा सरल और सरस है, भोजपुरी समाज को गैर-भोजपुरी भाषी इसी दृष्टि से देखते हैं. बॉलीवुड फिल्मों में भोजपुरी समाज के लोगों को सीधा, सपाट और निर्दोष दिखाया जाता है. पुरानी फिल्मों के नायक भोजपुरी बोलते हुए दिखते थे. अब वह स्थान फिल्मों में भोले-भाले और पान/दूध इत्यादि बेचने का काम करने वाले किरदारों को दे दिया गया है. भोजपुरी साहित्य को ऐसे अवमूल्यन से बचाने का प्रयास है इक्षु एकादश. अभी बात भोजपुरी के अस्तित्व के संघर्ष की नहीं, अपितु भोजपुरी में उत्कृष्ट साहित्य-सृजन की है.
नोबेल पुरस्कार विजेता ओल्गा तोकाचुर्क ने एक साक्षात्कार में कहा था, “अगर साहित्य वाकई कोई भूमिका निभाता है, तो मैं कहूंगी कि वह जानबूझकर नहीं निभाई जा रही होगी. अगर लेख केवल ‘एक्टिविज्म’ के लिए कोई उपन्यास लिखता है, तो यह अच्छा नहीं. आपको याद रखना चाहिए कि मैं कम्युनिस्ट काल में तगड़े प्रोपेगंडा को देखकर बड़ी हुई हूँ. मैं जानती हूँ कि प्रोपेगंडा कैसे काम करता है. यह एक लेखक, कलाकार, चित्रकार और तमाम रचनात्मक लोगों की ऊर्जा सोख लेता है, निगल जाता है.” पुस्तक के प्रधान सम्पादक और सम्पादक ने अपने शब्दों में भोजपुरी ‘एक्टिविज्म’ की कुछ बात की है लेकिन पुस्तक संग्रह की कवितायें किसी भी प्रकार के भाषाई दुराग्रह से मुक्त दिखती हैं. वास्तव में कवियों और लेखकों का संयमी और ईमानदार होना आवश्यक है जिससे वे अतीत और वर्तमान के यथार्थ को यथावत चित्रित कर सकें.
इस सन्दर्भ में इस पुस्तक की ‘चकबंदी क टीम’ कविता उल्लेखनीय है. “काँप गइल आपन परछाईं/थर थर काँप गइल/चकबंदी क टीम कभौं जब/अपने गाँव गइल.” समकालीन कविता की भाँति यह कविता गाँव में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक साहसी अभिव्यक्ति है. “नाहिं जाइब धान कटावे” में एक बिटिया, नारियों को देह-दृष्टि से देखने वाले पुरुषवादी मानसिकता का यथार्थ परोसते हुए कहती है, “खेत क मालिक बूढ़-जवनवां/टूकुर- टूकुर ताकैं/बिन खैनी क ठोंक गदोरी/झुट्ठे-मुट्ठे फाँकें/बोलें फूहर बात न देखें/ईहाँ बाटीं तिरिया.” यह “मी टू मूवमेंट” की ग्रामीण अभिव्यक्ति है. पूरब और पश्चिम के अपरिहार्य सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान ने उन्मुक्त यौन व्यवहार को बढ़ावा दिया है जिससे विगत कुछ वर्षों में स्त्रियों के विरुद्ध यौन अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. इन कविताओं ने उस साहित्यिक साहस और चेतना का परिचय दिया है जो समाज के लिए दर्पण का कार्य कर सकें.
“कलाकार समाज का निकटतम अंग है. इसलिए नये कवियों का प्रभावित होना सहज-स्वाभाविक है. समसामयिक परिस्थितियों से संपृक्त कविता में जन-जीवन के दुःख, नैराश्य, घुटन, उत्पीडन, विक्षोभ, बेचैनी, अनास्था और अनास्थाजन्य आक्रोश की सबलतम अभिव्यक्ति है.”
“बियाह” कविता में पुत्री अपने पिता से कहती है, “अमवा लगइहा बाबा बारी बगइचा/निबिया लगइहा दुआर/ पिपरा लगइहा बाबा पोखरा के भिटवां/गोइडे लगइहा बंसवार.” अनेक छंदों में पिता पुत्री का संवाद होता है, वह आम, नीम, पीपल के वृक्ष लगाने के लिए तैयार है क्योंकि वह पुत्री के तर्कों से सहमत है कि आम बड़ा होकर फल देगा, नीम छाँव और पीपल पर झूले लगेंगे. लेकिन वह बांस का वृक्ष लगाने के लिए तैयार नहीं होता है. “बंसवा से इ बेटी डोलवा फनाला/ होइ जाला घर सुनसान/बिटिया के बाबा से पूछा न कइसन/मड़वा कै होला बिहान.” केवल एक पुत्री का पिता यह जानता है कि पुत्री के विवाह में बांस सहायक सिद्ध होता है और अगली सुबह घर सुनसान हो जाता है. ऐसा ही भाव “झांके गोरी टारिके ओहार” नामक कविता में भी दृश्य है. इस काव्य संग्रह की सर्वाधिक संवेदनशील कविता “बियाह” है. इस संवेदना को संप्रेषित करने में कवि ने प्रकृति और मनुष्य के अन्योंयाश्रिता को बखूबी उजागर किया है. यह कविता आंचलिक कविता है.
“आंचलिकता का बोध वस्तुतः किसी क्षेत्र-विशेष के लोक-जीवन का, भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश में एक अध्येता के रूप में देखने की प्रवृत्ति का नाम है. इस दृष्टि से किसी भौगोलिक क्षेत्र-विशेष के लोक-जीवन के सुख-दुःख, जीवन विधि और लोकगीतों के प्रभाव को ग्रहण करके लिखी गयी कविताओं को आंचलिक कविता कहा जा सकता है. नयी कविता और नवगीत – दोनों में ही इस बोध की व्यंजना हुई है. पूर्वांचल के नवगीतकार गुलाब सिंह एक ऐसे गीत-हस्ताक्षर हैं जिनके गीतों में पूरा अंचल, पशु-पक्षी मनुष्य बोलते हुए से जान पड़ते हैं.” बियाह कविता का हिन्दी या अन्य भाषाओं में अनुवाद उन लोगों को समझ नहीं आ सकता है जो भोजपुरी माटी और लोक-जीवन की सुगंध से सर्वथा अपरिचित हैं. आंचलिक कविताओं को सर्वग्राह्य बनाने के लिए एक फुटनोट देना चाहिए जिससे पाठक सन्दर्भ समझ सकें.
‘गंगा गीत’ कविता भारतीय भूमि और भारतीय संस्कृति से गहरी संसक्ति का उद्घोष करती है. “सरग से आके उपकार मैया कइलू/तपसी भगीरथ के पुरखन के तरलू”. वाचिक परम्परा में यह कविता श्रोताओं के लिए अच्छी है. यह आस्था का गीत है, एक भक्त के लिए माँ गंगा की स्तुति है. परन्तु इस प्रकार के काव्य संग्रह में आस्था सार्वजनिक होते ही विवेक से टकराने लगती है. यहीं कविता सीमित हो जाती है और सार्वभौम नहीं हो पाती. राही मासूम रजा ने भी गंगा-प्रेम प्रदर्शित किया है लेकिन उनके प्रेम में एक विराट सन्देश छिपा है:
“मेरा नाम मुसलमानों जैसा है/मुझ को कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो/मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें मेरी बयाने जाग रही हैं/और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके/कालीदास के मेघदूत से यह कहता हूँ/मेरा भी एक संदेश है।
मेरा नाम मुसलमानों जैसा है/मुझ को कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो/लेकिन मेरी रग-रग में गंगा का पानी दौड़ रहा है/मेरे लहू से चुल्लू भर महादेव के मुँह पर फेंको/और उस योगी से कह दो-महादेव/अब इस गंगा को वापस ले लो/यह जलील तुर्कों के बदन में गढा गया/लहू बनकर दौड़ रही है।”
इस काव्य संग्रह में कुछ दार्शनिक कविताएं इसके वैविध्य को विस्तार देती है. “केतना चमकल केतना कडकल” इस संग्रह की प्रतिनिधि दार्शनिक कविता है. “जवन आज के विजय/पराजय पहुँचत काल्हि कहाय/विजय-पराजय के परिभाषा/बान्हत जात छिंटाय/कइसन जीतल-हारल/ऊंचा-नीचा मृण्मय भाव/हाड़-मांस हीरा-कोइला/कुल्हिये माटी के जात/रज के ढंके रजत भा/ढँकले रजत धुल जम जाय/जल में लहर-बुलबुला/कुल्हिये पानी के परिजन.” कविता भक्ति कवियों की भांति नश्वर संसार में निद्रामग्न मोहाच्छादित मनुष्य के लिए जागरण कविता है. प्यार, सहानुभूति, आत्मीयता इत्यादि धोखे के पर्याय हैं. धूमिल के शब्दों में, “वर्तमान समाज अब चल नहीं सकता/पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता.”
यह नानकदेव की कविता “बारू की भीत जैसी वसुधा को राज है” की अनुगूंज लगती है. परन्तु भक्त कवियों का समभाव और वैराग्य सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है. जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोजते हुए “आत्मजयी” में कवि कुंवर नारायण ने नचिकेता के माध्यम से जीवन को एक खोज बताया है. “जीवन केवल सुख की साधना नहीं/वह दिव्य शक्ति-अनवरत खोज/अनथक प्रयास/वह मुक्तिबोध/उस को पशु सा केवल तन से बाँधना नहीं”. इस काव्य संग्रह में “अंजोर ले ले अइह” में उजाला लाने की बात कही गयी है. “पिया अइह त/अन्हरिया में अँजोर लेले अइह/चान-तरई गढ़ौले पोरे पोर लेल अइह”. यह कविता अनथक प्रयास की बात करती है.
परन्तु इस नश्वर संसार की नश्वरता का भान करने वाले सांस्कृतिक प्रतीकों और आपसी संबंधों को बचाकर रखते हुए आधुनिक औद्योगीकरण व् विकास के यथार्थ के साथ संतुलन स्थापित करने की चुनौती है. ग्रामीण जनसंख्या नगरों में पलायन कर रही है. गाँव प्रधान और पंचायत के चुनावों के बाद मुकदमों और झगड़ों ने गाँवों को अजीबोगरीब बेतुके संसार में परिवर्तित कर दिया है. विकास के साथ मूल्यगत संक्रमण और विघटन की प्रक्रिया तीव्र हो गयी है. नगरों में रहने वाले कवि, विशेषकर गीतकार और नवगीतकार गाँवों की इस दुर्दशा से व्यथित हैं और पुराने समय को खोजते हैं.
प्रसिद्ध भोजपुरी कविता “गउवों गाँव बुझाते नइखे” की भांति इस संग्रह में संकलित कविता “घीउवा क दियना” आधुनिक गाँव में पुरातन रस्मों और प्रतीकों को खोजते हुए विकास की अंधी दौड़ को कोसती है. “तुलसी के चउरे प चउरा देखाला नाहीं/सँझिया ना दियना बराय/अब नाहीं गंगा क होखेला पुजनियाँ/अब ना पिरितिया नहाय”. इस गीत में वह स्मृतियाँ बुझी राख में चिंगारी सी हैं, रीते हुए पात्र की आखिरी बूँद हैं. उन्हें खो देने की व्यथा भोजपुरी गीतों में चित्रित ग्राम्य जीवन में भरी गूँज सी सर्वत्र परिव्याप्त हैं.
“…निराशा, पलायनवाद तथा ह्रास से ऊपर उठकर कलाकार का दायित्व नयी मर्यादा के स्थापन का होता है परन्तु यह दायित्व सुधारक या उपदेशक के स्तर का होता है. उसमें कला का अस्तित्व नहीं रह जाता. मूल्यों के विघटन के समय साहित्य-सृजन इसलिए कठिन अध्यवसाय तथा गहरी संवेदना की अपेक्षा रखता है. कलाकार को सामाजिक विकृतियों के बीच में रखकर पहले तो अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी पड़ती है और फिर नए मूल्यों तथा प्रतिमानों को निर्मित करना होता है…उपदेशक का कार्य हेय नहीं है पर कविकर्म उससे निश्चय ही भिन्न तथा दूसरे स्तर का है.” साहित्यकार समस्याओं का समाधान नहीं देता लेकिन समस्याओं का यथार्थ और सशक्त चित्रण पाठकों को समस्या के प्रति संवेदनशील बनाता है. समाधान की दिशा में यही साहित्यकार का महत्वपूर्ण योगदान है. पाठकों को भोजपुरी कवियों की संवेदना से रूबरू कराता यह भोजपुरी काव्य संग्रह एक सराहनीय प्रयास है. विषय और छन्द के वैविध्य ने इसे रोचक बनाया है. अनेक गीत वाचिक परम्परा और मंचन की दृष्टि से रचे गए हैं जिनके सौन्दर्य में कवि के स्वर संयोजन और प्रस्तुति का विशेष महत्व है. ऐसे गीत कागज पर बहुधा अपनी चमक खो बैठते हैं.
विविधता से भरे इस काव्य संग्रह में कुछ सशक्त कवितायें भी हैं. इन कविताओं में चिंता है, महत्त्व-चेतना है अतः वे अच्छी निर्मित हुई हैं. कतिपय गीत बिम्ब-योजना के कारण थोड़े दुरूह बन पड़े हैं. भोजपुरी शब्दों के ईक्षुवत रस-माधुरी की प्रचुरता पुस्तक में बिखरी हुई है. यहाँ सामूहिक निराशा भी है और जीवन की विषम परिस्थितियों के बीच मनुष्य की जिजीविषा का संकेत भी. कहीं भ्रम है, कहीं नैराश्य, कहीं प्रेम और कहीं उत्साह बढाते गीत. कहीं फाल्गुन के रंगों में जीवन झूमता है तो कहीं जमीन की कवितायें जमीन से सहज जोड़ देती हैं. प्रेम अपने सघन ऐन्द्रिक पार्थिव स्वरूप में भी विद्यमान है और इन्द्रियों का अतिक्रमण करते हुए अमूर्त स्वरूप में भी. भोजपुरी पाठकों के लिए यह काव्य संग्रह महत्वपूर्ण और पठनीय है. अंत में , त्रिलोचन के शब्दों में,
शब्दों में भी हाड़-मांस है, जीवन धरकर
वे भी जीवधारियों के स्वर-यंत्र संभाले
स्फुट, अस्फुट दो धाराओं में प्रवहमान हैं.
भूतपूर्व छात्र: बैचलर ऑफ़ इंजीनियरिंग (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला), मास्टर ऑफ़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापोर, आई आई एम अहमदाबाद)
लेखक: शिखा (काव्य संग्रह, २०००), कामरेडों को मूर्ति पूजा नहीं आती (काव्य संग्रह, २०२१)]